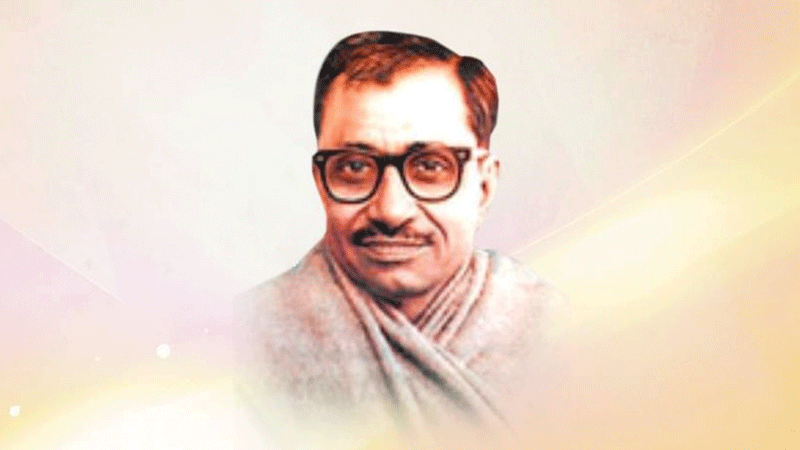दीनदयाल उपाध्याय
हम अपने राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। या जैसे कि प्रतिज्ञा में कहा गया है कि हम उसकी सर्वांगीण उन्नति देखना चाहते हैं। वैभव की यह अवस्था कैसी होगी? उन्नति की यह स्थिति कैसी होगी? इसकी कुछ कल्पना भी हमने प्रतिज्ञा और प्रार्थना दोनों में करके रखी है। वह अपने धर्म के आधार पर, क्योंकि हमने यह कहा है कि इस धर्म की रक्षा करते हुए हम इसे परम वैभव पर ले जाएं अर्थात् यदि धर्म का विस्मरण कर दिया और यह कल्पना भी कर लें कि हमें किसी भी प्रकार का वैभव प्राप्त हो गया तो हम उसे नहीं मानेंगे।
दूसरी बात जो इससे भी अधिक सत्य है कि राष्ट्र का वैभव बिना धर्म का आधार लिए प्राप्त नहीं हो सकता। बिना धर्म की रक्षा किए वह वैभव नहीं मिल सकता। किसी वस्तु का वैभव उसके धर्म को भुलाकर कभी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार अपने राष्ट्र के वैभव के संबंध में, इसके साथ ही हमने यह विचार किया था कि जब हम इस धर्म शब्द का उपयोग करते हैं तो उसकी सामान्य कल्पना क्या है? उसके नाते धर्म की जो एक व्याख्या हमने की, उसका आधार यह कि धारणा से धर्म शब्द प्रचलित हुआ था। जिससे धारणा होती है, जिस शक्ति से, जिस तत्त्व से, जिस प्रवृत्ति से, जिस व्याख्या से जिस किसी भी चीज़ की धारणा हो सके वह धर्म है।
प्रजा की धारणा भी होती है और इस नाते से हम किस आधार पर टिके हुए हैं, जब इसका विचार किया तो उसमें यह भी देखा कि शरीर को टिकाए रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक हैं, वह सब धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी। समाज कार्य के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, वह समाज धर्म के अंतर्गत आ जाएंगी। समाज और शरीर इन सबको टिकाए रखने के लिए जितनी भी चीजें ज़रूरी हैं, वे सब अपने धर्म के, सृष्टि के अंतर्गत आ जाएंगी। इस प्रकार से यह धर्म केवल उसकी एक इकाई है। जो भिन्न-भिन्न इकाइयां हैं, इन सब इकाइयों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। यदि उसके बीच में कोई संघर्ष आ गया, कोई विरोध उत्पन्न हो गया, किसी भी कारण क्यों न हो, विरोध को मिटाकर उसके स्थान पर समन्वय करके धर्म की प्रतिष्ठापना करना, उसके लिए प्रयत्न करना और दोनों प्रकार की इकाइयां, सभी इकाइयां सामान्य आधार के ऊपर अपना विचार प्रकट कर सकें, अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें, एक-दूसरे के साथ पूरकता के भाव से काम कर सकें, वह काम ही वास्तव में धर्म का काम है।
जैसे यदि एक व्यक्ति के शरीर का विचार करते हैं तो शारीरिक दृष्टि से उसकी जो इंद्रियां हैं, वे एक-दूसरे के लिए पूरक हैं। सबका योग्य विकास हो सके, आपस में संघर्ष न आए, वैसे ही एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में कोई संघर्ष न आए और जो व्यक्तियों के समूह बनते हैं, उनके बीच में कोई संघर्ष न आए। विभिन्न प्रकार के बने हुए व्यक्तियों के समूहों के बीच में संघर्ष न आए। संपूर्ण प्राणिमात्र और मानव उनके बीच किसी प्रकार का संघर्ष उपस्थित न हो। संपूर्ण प्राणी जगत् और प्रगति के बीच में किसी प्रकार का संघर्ष उपस्थित न हो, बल्कि सब एक-दूसरे के लिए पूरकता का भाव लेकर विकास के लिए विचार करते हुए आगे बढ़ें। इस प्रकार की यह स्थिति सामान्य है। हमारा धर्म एकांगी नहीं, वह तो सर्वांगीण है, व्यापक है, सबका विचार करके चलने वाला है। यह हम लोगों का सामान्य विचार रहा है।
अन्य दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में और भी विचार हैं। पश्चिम के भी अनेक विचार हैं। अनेक विचारों के साथ तथा हमारे इस विचार के साथ मूलतः एक मतभेद खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम इस प्रकार से एक इकाई और दूसरी इकाई के बीच सामंजस्य मानकर चलते हैं। परंतु पश्चिम में जो प्रमुख विचार हुआ है, वह यह कि उनके सभी प्रयत्नों में विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य नहीं। वहां उन्होंने विरोध को प्रथम स्थान देकर रखा है। उनकी सामान्य कल्पना संपूर्ण जीवन के संबंध में यह रही है कि मानव का जीवन संघर्षमय है। इस संघर्ष में से ही कुछ पीढ़ियां समाप्त होती चली जाती हैं। बाक़ी जो हैं, वही प्रगति करती चली जाती हैं। सृष्टि भी इसी संघर्ष के आधार पर खड़ी हुई है। यानी वहां के जीवन में आधार पर विचार करें। अंग्रेजी में एक शब्द को लें तो उनकी संपूर्ण Philosphy Competition (प्रतिस्पर्धा) के ऊपर आधारित है। यही उनका विचार चलता है। अपनी जितनी भी विचारधारा है, वह सहयोग के ऊपर आधारित है। पूरकता पर आधारित है। यहां पर Competition का विचार नहीं है। जीवन का आधार Co-operation है। सहयोग, सहकारिता आधार है। पूरकता का आधार है, इसको हम मानकर चलते हैं।
वहां इस प्रकार का विचार न करके उन्होंने Competition के विचार को ही प्रमुखता आज भी दी है। दूसरी बात जो उन्होंने विचार किया है वह यह किया है, कि जहां हम प्रत्येक इकाई का विचार उसकी पूर्णता को देखने में करते हैं, वहां उन्होंने इकाई को पूर्णता की दृष्टि से नहीं देखा। उदाहरण के लिए यदि शरीर को लें तो हम व्यक्ति के शरीर को केवल भौतिक आवश्यकताओं का पुंज मात्र मानकर नहीं चलते। भौतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ उसकी और कौन-कौन सी आवश्यकताएं भी हैं, उसकी सब प्रकार की हस्तियां हैं। इस वस्तु को मानकर हम चलते हैं, परंतु पश्चिम के अनेक लोग केवल भौतिक दृष्टि से तैयार रहें, जो मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसी के संबंध में विचार होता है। इसके अतिरिक्त दूसरा विचार ही नहीं आता। भौतिक और बाक़ी की आवश्यकताएं हैं, इन आवश्यकताओं को प्रमुखता व बाक़ी को गौण स्थान देकर वे चलते हैं। व्यक्ति और समाज के बीच संघर्ष आते हैं और आ सकते हैं। यह उनका स्वाभाविक और सामान्य विचार है। यदि इस प्रकार के संघर्ष आकर खड़े हो जाते हैं तो वह एक असामान्य स्थिति है। वह धर्म की स्थिति नहीं है, तो एक प्रकार से विकृति की स्थिति है। ऐसा हम विचारकर चलते हैं। जैसे कि अपने दोनों पैर हैं। दोनों पैर भगवान् ने इसलिए बनाए कि वे ठीक प्रकार से चलें। आपस में लड़ते नहीं, टकराते भी नहीं, और दोनों पैरों का उपयोग भी हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। दोनों पैरों में कौन आगे जाएगा और कौन पीछे जाएगा, इसका विचार नहीं करते, झगड़ा भी नहीं होता।
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य यदि कमज़ोर हो गया तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जिन पैरों का काम यह है कि मनुष्य के संपूर्ण शरीर के बोझ को संभालकर चलें, जिन पैरों का काम संतुलन बनाए रखना है, वे पैर भी उसके संतुलन को बिगाड़ देते हैं। ऐसी स्थिति कभी-कभी आती है, परंतु वह स्थिति हमारी कमज़ोरी के कारण होगी। आहार-व्यवहार में कुछ बिगाड़ से उत्पन्न हुई, किंतु यह सामान्य स्थिति नहीं। यह असामान्य स्थिति है और उस असामान्य स्थिति को दूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए यदि कोई इस असामान्य स्थिति को सामान्य स्थिति कहकर चले और यही सोचकर चले कि पैरों का काम ही लड़खड़ाने का है। पैर लड़खड़ाएं नहीं, इसलिए लकड़ी की पट्टी बांध दें, यदि इस प्रकार का कोई विचार करके चलेगा, तो मूलत: वास्तव में अलग विचार होगा। ऐसा लगता है कि पाश्चात्य जगत् के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ इसी आधार पर अपने संपूर्ण जीवन की रचना की है और उसमें फिर अपना-अपना स्वार्थ रखकर दोनों के बीच प्रतियोगिता को आधार बनाकर प्रतिदिन बराबर करते गए और उसमें से व्यक्ति और समाज के बीच एक संघर्ष खड़ा किया। पश्चिम के लोग व्यक्ति और समाज के बीच एक संघर्ष खड़ा है, ऐसा मानकर चलते हैं। इसलिए आज वहां पर दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं : एक ऐसे, जो व्यक्ति को प्रमुखता देकर समाज को पीछे डालकर कहते हैं कि व्यक्ति प्रमुख है।
समाज जो कुछ करेगा, व्यक्ति के हितों के लिए करेगा और समाज को वहीं तक मानने को तैयार हैं, जहां तक व्यक्ति के लिए वह सहायक है। इस प्रकार का विचार रखनेवाले लोग पश्चिम जगत् में दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ़ ऐसे लोग हैं जो ऐसा विचार रखते हैं कि यदि कुछ व्यक्तियों ने गड़बड़ की तो उस गड़बड़ के आधार पर यह मानकर कि सारे व्यक्ति खराब हैं और यह व्यक्ति समाज के संबंध में विचार नहीं कर सकते, ये लोग दूसरों के हित का विचार नहीं कर सकते, इसलिए इनकी सत्ता को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। वे समाज को ही प्रमुख स्थान देकर जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानकर चलते हैं, व्यक्ति को मान का स्थान दिया तो समाज समाप्त हो जाएगा। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यदि समाज को प्रमुखता दी, व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज का हित–ये दोनों मानो साथ नहीं चल सकते। दोनों में से हमें एक को चुनना पड़ेगा। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए तो समाज के हित की चिंता नहीं करनी चाहिए। समाज के हित की सोचने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में समाज को समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार का विचार करनेवाले लोग वहां पर पैदा हो गए।
वे सही विचार नहीं करते हैं। मानव और बाक़ी के अन्य प्राणियों–इन सबके बीच मानो एक प्रकार का संघर्ष है। संघर्ष में मानव को अधिकार है, सभी अन्य प्राणियों का उपयोग अपने लिए करे। अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई है, केवल शक्ति की होड़ है। डार्विन ने विचार किया और कहा कि यहां पर Survival है। जो योग्य हैं, वही ठीक क्रम में हैं, बाक़ी जितने अयोग्य हैं, एक-दूसरे को खाते चले जाते हैं। अपने जीवन को बनाए रखने की लड़ाई और इस लड़ाई में संघर्ष ही इसका प्रमुख आधार है। कुछ और आगे विचार करते चले जाएं तो यह देखेंगे कि उनकी दृष्टि में मनुष्य और प्राणियों के बीच तथा मनुष्यों में संपूर्ण मानव समाज, छोटे-छोटे गुट हैं, राष्ट्र हैं और राष्ट्रों में और राष्ट्र और व्यक्तियों के बीच में, व्यक्ति की भी जो अनेक प्रकार की हस्तियां हैं, उन सबके बीच में मानो एक परमानेंट संघर्ष की स्थिति है।
क्रमश:
-संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : हरिगढ़ (5 जून 1962)