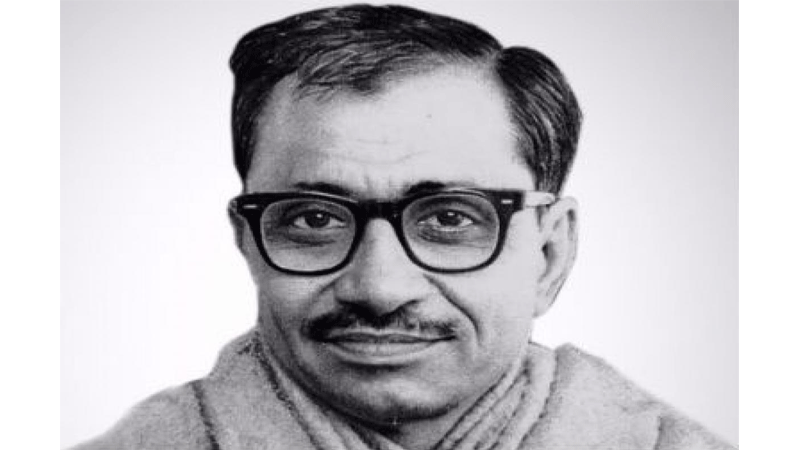दीनदयाल उपाध्याय
हमें अपने जीवन के लिए परानुकरण की आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपनी ही परंपरा का विचार करके अपनी जीवन रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा राष्ट्र कोई सद्य उत्पन्न राष्ट्र नहीं है। हमारा सहस्रों वर्षों का इतिहास है, हमारी स्वयं की एक जीवन पद्धति है. जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती है. पर हां, यह बात अवश्य है कि हज़ारों वर्षों के इतिहास में हमारे यहां जो जीवन पद्धति चली है। उसको हम आज वैसा का वैसा लेकर नहीं चल सकते। क्योंकि कुछ-न-कुछ युग का भी विचार करना पड़ेगा। यदि हम आज अपनी प्राचीन जीवन पद्धति को उसके असली रूप में अपनाना चाहें तो हम नहीं कर सकते। हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आ जाएंगी, परंतु हमारी जीवन पद्धति के पीछे जो तत्त्व हैं, हम उनको भुलाकर काम नहीं चला सकते। हमें उनके मूल रूप पर विचार कर उन्हें युगानुकूल बनाकर ग्रहण करना होगा।
जब हम तात्त्विक भूमिका के आधार पर खड़े होते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रश्न उठते हैं-जैसे मनुष्य क्यों पैदा होता है? उसका लक्ष्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए? हम जब भी किसी चीज़ का विचार करते हैं तो उसका विचार हमें इस आधार पर करना पड़ता है कि यह हमें किस लिए चाहिए ?
जिसे रेलगाड़ी से जाना है, उसे तो उन्हीं साधनों का विचार करना पड़ेगा, जो उसकी यात्रा में आवश्यक हैं, परंतु जो कहीं जाने वाला नहीं, यदि वह यात्रा की आवश्यक वस्तुएं जुटाने का प्रयास करेगा तो यह ठीक नहीं होगा। इसी तरह हमारी जीवन की यात्रा है। यह यात्रा कहां से प्रारंभ होगी? कहां पर समाप्त होगी? इस पर विचार करने पर हम कुछ बातें पाते हैं। मनुष्य अपनी जीवन यात्रा में कुछ चीजें करता है, कुछ नहीं करता। जो सुखकारक है वह करता है, जो सुखकारक नहीं वह नहीं करता है। अब प्रश्न उठता है कि ‘सुख’ है क्या? व्यावहारिक रूप से इसका विवेचन करने के लिए एक दूसरा प्रश्न उठता है कि यह सुख किसका? तो हम कहेंगे कि इंद्रिय का सुख; पर इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। केवल इंद्रिय सुख से ही काम नहीं चलता। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम इंद्रियों के सुख की वस्तु को त्याग देते हैं। उदाहरण के लिए हम भोजन करते हैं तो इंद्रिय सुख मिलता है, पर क्या हम शत्रु के यहां भोजन करेंगे?
मानसिंह ने राणाप्रताप के यहां भोजन नहीं किया। हम सोचें, आख़िर क्यों नहीं किया? क्या वहां भोजन करने पर उसे इंद्रिय सुख नहीं मिलता? पर नहीं जो हमारा शत्रु है, जिससे हमारा मनमुटाव हो गया, जो अपना तिरस्कार करता है, अपना अपमान करता है, हम उसके यहां भोजन नहीं करते। इससे यह आवश्यक नहीं कि वहां भोजन करने से हमें इंद्रिय सुख नहीं मिलता; इंद्रिय सुख तो मिलता है, पर मन गवाही नहीं देता, मन को सुख नहीं मिलता। अतएव सुख का संबंध केवल इंद्रियों से ही नहीं, मन से भी है, मन के सुख को हम बुद्धि का सुख कहते हैं। बुद्धि को भी सुख की ज़रूरत होती है। बुद्धि को भी शक्ति की ज़रूरत होती है। एक पागल व्यक्ति कई बार हृष्ट-पुष्ट भी हो जाता है, कई बार उसे सुख भी होता है, परंतु उसकी बुद्धि अविकसित रहती है, उसकी बुद्धि में कष्ट रहता है और इस कष्ट के कारण उसे खाने-पीने के बाद भी चैन नहीं रहता, अर्थात् सुख मन का चाहिए, बुद्धि का चाहिए, और इसके आगे भी आत्मा का चाहिए। साधारणतया हम यह मानकर चलते हैं कि जब हम सुख की कल्पना करते हैं तो उसमें सभी इंद्रियों का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख एवं आत्मा के सुख का संयोग होना चाहिए। जिन साधनों द्वारा ऊपर कथित चार तत्त्वों का पूर्ण विकास हो सके-वही हमें अपनाना चाहिए, जिससे सुख प्राप्त हो सके।
सुख प्राप्ति के लिए जिन साधनों को अपनाने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, उन्हें हमारे यहां ‘पुरुषार्थ’ कहा गया है। वह पुरुषार्थ-धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष-चार प्रकार का हो सकता है। ये चारों ‘पुरुषार्थ’ एक-दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थ पुरुषार्थ शरीर के लिए, धर्म पुरुषार्थ समाज के लिए, काम पुरुषार्थ कामना के लिए और मोक्ष पुरुषार्थ आत्मा के लिए-अर्थात् इन चारों पुरुषार्थों के समावेश से ही मनुष्य उन्नति कर सकता है। मनुष्य जब चारों के लिए प्रयत्नशील होगा, चारों की प्राप्ति का प्रयास करेगा तो उसे सुख मिल सकेगा। अब विचार होता है कि क्या कोई एक पुरुषार्थ ऐसा है, जिसकी प्राप्ति हो और शेष सारी चीजें स्वयं प्राप्त हो जाएं? अपने यहां अनेक लोगों ने इसके भिन्न उत्तर दिए हैं और सभी अपने-अपने उत्तर को महत्त्व देते हैं। जैसे कॉलेज में अर्थशास्त्र या तर्कशास्त्र पढ़ाने वाला अपने ही शास्त्र को प्रमुख शास्त्र कहता है, उसी तरह यहां भी कोई कहता है कि ‘अर्थ’ ही प्रमुख है तो कोई कहता है कि प्रमुख है तो ‘काम’; किसी ने कहा कि धर्म प्रमुख है तथा किसी ने ‘मोक्ष’ को महत्त्व दिया। अनेक बार ऐसा विवाद हुआ है कि हमें धर्म को आधार मानकर चलना चाहिए तो अर्जुन ने कहा कि अर्थ सबसे बड़ा है, उसके बिना धर्म नहीं चलेगा।
जब हम ‘अर्थ’ शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र दोनों आ जाते हैं-यद्यपि यह दोनों मिलकर भी अर्थ पुरुषार्थ को पूरा नहीं करते। यद्यपि कुछ चीजें अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र की हैं, किंतु उनका समावेश अर्थपुरुषार्थ में नहीं होता। अर्थ सब चीजों का आधार है, धर्म उसी पर टिकता है। अर्थ नहीं रहेगा तो धर्म नहीं चलेगा, अतएव राज की भी आवश्यकता, इसी आधार पर प्रतिपादित की गई है और उसी के आधार पर धर्म हमारे यहां चलता है।
यदि धर्म का समाज हो जाएगा, तो धर्म ही समाज हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में अर्थ होगा तो सभी चीजें ठीक होंगी। कहते हैं कि विश्वामित्र जब भूखों मरने लगे तो चांडाल के यहां से कुत्ते का जूठा मांस चोरी करके खाया। चांडाल के शंका करने पर उन्होंने कहा, इसमें अधर्म कुछ नहीं है। सब धर्मों का आधार प्राण रक्षा है। सुख प्राणों को तृप्त करने वाली चीज़ को कहते हैं। प्राण को धर्म का आधार कहा और प्राण रक्षा अर्थबाहुल्य से ही संभव है। जिसके पास अर्थ नहीं उसको मां-बाप, भाई-बंधु कोई नहीं पूछते, पर इस अर्थ में यदि धर्म का भाव छोड़ दिया तो अनर्थ हो जाना स्वाभाविक है।
राज्य केवल इसलिए आया कि वह धर्म को चलाकर चले। शास्त्रकारों ने अर्थ को सबका मूल कहा। कुछ ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी वस्तु काम है, यह न रहा तो सब चीज़ बेकार है। विदुर ने कहा कि अर्थ बंधन कारक है, धर्म बंधन कारक है और काम तो बंधन कारक है ही। सबसे बड़ी वस्तु मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता, फिर कोई कामना भी नहीं रहती। इसलिए निष्काम भाव से मोक्ष पा लेना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। विदुर के इस विवाद का अंत युधिष्ठिर ने किया। उन्होंने कहा कि कोई भी एक पुरुषार्थ बड़ा नहीं है। चारों को जो एक साथ लेकर चलेगा, वही पुण्य है। एक को पाने का जो प्रयास करेगा, वह अधूरा है और एक को प्राप्त करने का प्रयास करने वाला पापी भी है। एक को विचार करना मानव जीवन के टुकड़े करना है, किंतु यह सत्य है कि मानव-जीवन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। कई बार शास्त्र खंड-खंड करके विचार करते हैं, जिसके कारण ग़लती होती है; क्योंकि वह विचार जीवन के एक अंग के बारे में रहता है। पश्चिम में इसी प्रकार टुकड़े-टुकड़े करके विचार हुआ।
‘पोलिटिकल’ है तो केवल ‘मैन इज़ ए पोलिटिकल बीइंग’ का विचार करेगा। ‘इकोनॉमिक्स’ में ‘इकोनॉमिक मैन’ की कल्पना की गई, जिसका एक ही जीवन है और जिसमें अर्थशास्त्र की क्रियाएं एवं सिद्धांतों का ही विचार होता है। जबकि वास्तविक जीवन में ऐसा होता नहीं। आर्थिक क्रियाओं के पीछे केवल अर्थ एवं उपयोगिता के सिद्धांत काम नहीं करते, वरन् कुछ और भी भावनाएं काम करती हैं, जैसे अपने देश में बनी वस्तु महंगी होने पर भी, कम उपयोगी होने पर भी ख़रीदी जाती है। इसी प्रकार जब बालक बढ़ जाता है तो उसकी इच्छित वस्तु ख़रीदनी ही पड़ती है, चाहे उपयोगिता की दृष्टि से न्यून ही क्यों न हो। ऐसे समय में यदि हम अर्थशास्त्र का ही विचार करें तो अनर्थ हो सकता है। वास्तविकता यह कि हमें मानव-दृष्टि से विचार करना चाहिए। मनुष्य की अनेक भावनाएं हैं। केवल एक मनोवृत्ति का ही विचार न करें, तब तो चारों पुरुषार्थों को समान मानकर हमें चारों की उपासना करनी चाहिए।
इन चारों का आधार स्तंभ यदि कोई हो सकता है तो वह धर्म ही है। धर्म से अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है। यद्यपि धर्म, अर्थ एवं काम पर टिकता है, पर यदि इसमें से धर्म को छोड़ दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और यदि उसमें धर्म जोड़ दिया जाए तो वही अर्थ हमारे काम की प्राप्ति का साधन होगा। धर्म, अर्थ एक-दूसरे के पोषक होते हैं। मनु ने धर्म के दस लक्षण गिनाए हैं-धृति, क्षमा, दमोस्तेयम्। भूमि इन्हीं के आधार पर अर्थ की प्राप्ति होती है। धृति (धैर्य) जो कि धर्म का बिल्कुल आधार है, मानव इसी धृति को आधार मानकर चलते हैं। ‘धारणात् धर्म इत्याहुः’ में धृति पहली चीज़ कही गई है, जो कि किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। धनार्जन में भी धैर्य रखना आवश्यक होता है, जो धैर्य रखकर प्रयत्न नहीं कर सकता, वह पैसा भी कमा नहीं सकता।
धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। जो व्यवहार में अच्छा है और व्यवहार में कोई बात आ गई तो गम खा लेगा, लड़ेगा नहीं, ऐसा क्षमाशील है-शायद क्षमा व्यापार वृद्धि एवं अर्थार्जन के लिए भी आवश्यक है। जो दूसरों के अवगुण को क्षमा करके चल नहीं सकता, वह अर्थार्जन भी नहीं कर सकता। दुकान पर आने वाला ग्राहक चाहे ग़लत बोल बोले, दुकानदार को भला-बुरा कहे, दस रुपए की वस्तु के दो रुपए लगाए, पर अच्छा दुकानदार इससे कभी बुरा नहीं मानता। धर्म का तीसरा लक्षण सत्य है। सत्य का अर्थ है, मन-वचन-कर्म की एकता। आजकल लोग सोचते हैं कि व्यवसाय में असत्य ही चलता है, पर यह ग़लत है। सत्य को यदि जीवन से निकाल दिया जाए तो कुछ काम नहीं चल सकता। पारस्परिक विश्वास सत्य के आधार पर ही संभव है। इस सत्य से हमारा व्यवसाय भी बढ़ता चला जाएगा। हम अधिक धनार्जन करने में सफल हो सकेंगे। यदि हमने सत्य का पालन नहीं किया तो व्यवस्था में पूर्ण गड़बड़ी आ जाएगी।
आज की जो व्यावहारिक कठिनाइयां देखते हुए व्यवसायी लोग भी मिलावट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर धार्मिक भावना लुप्तप्राय हो गई है। इन सब बातों का संबंध हमसे है, अतएव हमें धर्म के आधार पर चलना होगा; अपने जीवन में सत्य, धर्म को सम्यक् प्रकार से प्रतिष्ठित करना होगा। सारांश यह कि धर्म से अर्थ का घनिष्ठ संबंध है तथा धर्म से हर अर्थ की प्राप्ति संभव है। दूसरी ओर अर्थ से धर्म टिकता है। यदि अर्थ प्रचुर मात्रा में हुआ तो धर्म का ठीक प्रकार से पालन होता है अन्यथा इसके अभाव में लोग परस्पर लड़ते हैं, अधर्म होता है। यदि गाड़ी में पर्याप्त स्थान है तो कोई गड़बड़ी नहीं मचती, पर यदि जगह का अभाव हुआ तो गड़बड़ी मचती है, उठने वालों को उतरना मुश्किल हो जाता है, फिर वह तो उतरेगा ही-किसी के पांव पर पांव रखकर; किसी को कुचलते हुए उतरते हैं। अब अभाव के कारण ‘क्यू हैबिट’ का विचार आता है। भारत में ‘क्यू हैबिट’ नहीं है, पर जहां अभाव नहीं, वहां ‘क्यू हैबिट’ की क्या आवश्यकता? क्यू हैबिट’ की आवश्यकता अभाव में होती है। जब सबके पास पर्याप्त खाने को है तो राशनिंग की क्या आवश्यकता? अतएव हमारे यहां जो नियम बने, वह समृद्धि काल को याद दिलाते हैं, अर्थात् जिस समय हमारे यहां नियम बने, उस समय देश समृद्ध था।
-पाञ्चजन्य, अक्तूबर 10, 1960 (क्रमशः)