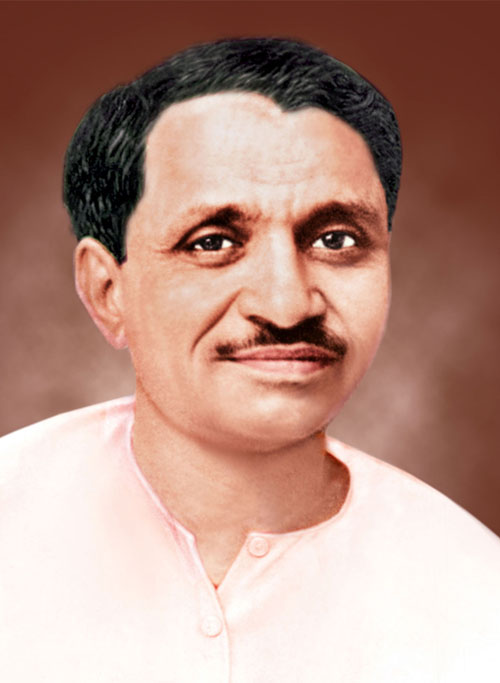राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात् आज सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने अर्थ का है। सामाजिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम उसके आर्थिक पहलू पर भी विचार करें। हमारे आर्थिक मूल्य क्या हैं और जीवन के किन मूल्यों के आधार पर हम समाज को सुख, श्री और समृद्धि से संपन्न कर सकते हैं- इन प्रश्नों पर भी विचार करना अवश्यक है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमारे आर्थिक और भौतिक जीवन के विकास की भी समुचित व्यवस्था की गई है। जो यह बात सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति तो केवल अध्यात्मवाद पर ही जोर देती है तथा भौतिक उन्नति को उसमें कोई स्थान नहीं, उनकी यह धारणा बिल्कुल ही निर्मूल है। भारतीय संस्कृति में भौतिक विकास के लिए उतना ही स्थान है, जितना आध्यात्मिक विकास के लिए। हमारे अपने आर्थिक मूल्य हैं; अपनी अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था का देश और काल दोनों से ही संबंध है। इसलिए हमारे यहां युगधर्म और राष्ट्रधर्म दोनों की बात स्पष्ट रूप से कही गई है।
राष्ट्रधर्म
आज युग की दृष्टि से हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे भौतिक साधनों का भी विकास हुआ है। अतरराष्ट्रीय समानता की बात भी हम कहते हैं। परंतु तथ्य फिर भी कुछ और है। प्रत्येक राष्ट्र के भिन्न-भिन्न स्तर हैं। वे अपने राष्ट्रीय हित की दृष्टि से ही विचार करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक और भौतिक साधन भी भिन्न-भिन्न हैं। अत: हम अंतरराष्ट्रीय समानता के आधार पर युगधर्म की बात कहकर राष्ट्रधर्म को भुला नहीं सकते।
मानसिक वृत्तियां और आर्थिक प्रयत्न
एक बात और, आर्थिक पहलू पर विचार करते समय लोग मानसिक प्रवृत्तियों पर विचार नहीं करते, जबकि हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर मानसिक प्रवृत्तियों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रवृत्तियां सांस्कृतिक जीवन से प्रभावित होती हैं। अत: हमारे आर्थिक प्रयत्नों पर संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव रहता है। हमारी संस्कृति में भी हमारे आर्थिक प्रयास किस आधार पर चलें, इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है; भौतिक विकास के लिए उसमें समुचित स्थान है।
आर्थिक विकास को स्थान
हमारे धर्म में पग-पग पर इहलोक और परलोक बनाने की बात कही गई है। इसलिए हमने लक्ष्मी को देवी स्वरूपा माना है, उसमें देवत्व की स्थापना की है। इसलिए हम उसे काम्य और भोग्य भाव से न देखकर पूज्य और श्रद्धा भाव से देखते हैं। ‘वंदेमातरम्’ में भी जब हम भारतमाता की वंदना करते हैं, सबसे पहले उसका ‘सुजलां, सुफलां, मलयज शीतलाम्’ वाला रूप ही हमारे सामने आता है, अर्थात् (प्रथम हम उसकी भौतिक श्रीसमृद्धि का ही विचार करते हैं, उसके अन्य रूपों की कल्पना तो बाद में ही की जाती है। अत: भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ की बात कहकर हम यह तो कह ही नहीं सकते कि इस संस्कृति में केवल अध्यात्म और ब्रह्म पर ही विचार किया जाता है तथा मौलिक विकास को पूर्ण रूप से उपेक्षित किया जाता है। अब जब भौतिक विकास की बात को हमारी संस्कृति प्रतिपादित करती है तो उसके लिए उसकी समुचित व्यवस्था भी की गई है। हमारा अपना एक आर्थिक दर्शन है, उसके आधार पर हमारे मनीषियों ने आर्थिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन व्यवस्थाओं में भिन्नता मिल सकती है, क्योंकि मनु महाराज ने यदि अभिनवीकरण का बहिष्कार किया है तो कौटिल्य ने उसका प्रतिपादन, परंतु दोनों का दर्शन फिर भी एक है। अत: हम उसके व्यावहारिक पहलू पर विचार न कर दार्शनिक पहलू पर ही विचार करें। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए जैसा कि पूर्व भी कहा जा चुका है, हमारे यहां युगधर्म और राष्ट्रधर्म दोनों की अलग-अलग बात कही गई है, अर्थात् युग और देश की परिस्थिति के अनुसार ही हम अपनी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करें।
संपत्ति का अधिकार
अब हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह उठता है कि समाज में संपत्ति पर किसका अधिकार हो। कुछ लोग यह नारा लगाते हैं कि ‘कमाने वाला खाएगा’। एक दृष्टि यह ठीक भी है, क्योंकि यह मनुष्य की प्रकृति है। अर्थशास्त्र इसी का प्रतिपादन करता है। परंतु मानव और समाज कल्याण के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए स्वयं कर्म करके, उसके फल को स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक दूसरे को अर्पण कर देने के भाव का आदर्श भी आवश्यक है। यही संस्कृति है, परंतु इस प्रकार की संस्कृति आज व्यवहार में कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती और प्रकृति का केवल नारा भर लगाया जाता है। व्यवहार में आज इन दोनों से भिन्न एक तीसरी चीज़ ही सामने है-विकृति अर्थात् कर्म तो कोई करे कमाए कोई, और खाए कोई अन्य। यह ज़बरदस्ती ही आज चारों ओर दिखाई देती है। यही विकृति है। परंतु भारतीय संस्कृति प्रकृति से भी ऊपर उस परम आदर्श पर बल देती है, जिसको गीता के कर्म के सिद्धांत में व्यक्त किया गया है-अर्थात् फल की भावना से रहित होकर कर्म करो और उससे अर्जित फल को भगवतार्पण कर दो। भगवान् अर्थात् समाज। ईश्वर का प्रत्यक्ष और विराट् स्वरूप आज समाज ही है। वही विराट् पुरुष है-यही मानकर हम चलें और अपने समस्त कर्मो के फल हम समाज को अर्पण कर दें।
हमारी समाज कल्पना
अब जब समाज की बात उठती है तो उसके विषय में भी हमारी कल्पना स्पष्ट हो जानी आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के अनुसार समाज के बहुत से रूप हैं। रूस के अनुसार उसका ‘स्टेट’ रूप में कभी प्रयोग नहीं होता और न उसमें रूस की विचारधारा के अनुसार राष्ट्रीयकरण को ही महत्त्व दिया जाता है। भारतीय समाज रचना में व्यक्ति अर्थात् व्यष्टि को प्रमुख स्थान दिया गया है। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। हम समाज में व्यक्ति और परिवार से लेकर ग्राम, राष्ट्र और अखिल विश्व तक की कल्पना करते हैं। इसलिए जो कुछ हम उत्पन्न करें, उसे संपूर्ण राष्ट्र के हित में व्यय कर दें। राष्ट्र ही हमारे कर्म की प्रेरणा का स्रोत रहे। यही भावना भारतीय संस्कृति के आर्थिक रूप का मूल आधार है। इसी आधार पर हम समाज को सुख, श्री और समृद्धि से संपन्न बना सकते हैं और यह तभी संभव है जब हम भारतवर्ष को कर्मभूमि मानकर चलें, भोगभूमि नहीं। जहां भोग की भावना आ जाती है, वहां परिश्रम और कर्म चाहे स्वयं ही क्यों न किया जाए एक पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण हो जाता है, वह हमें मान्य नहीं, क्योंकि ‘प्रकृति’ होते हुए भी वहां ‘जंगल का क़ानून’ होता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ ही प्रधान होता है तथा समाज और राष्ट्र का सामूहिक हित गौण पड़ जाता है। वहां फिर ठीक वितरण नहीं हो पाता और समाज के सामूहिक विकास का मार्ग सिमटकर कुछ लोगों की पकड़ में चला जाता है। अत: राष्ट्र की चिंता को प्रधान मानकर हम अपनी ‘प्रकृत’ अवस्था से भी ऊपर उठकर ‘संस्कृत’ अवस्था को प्राप्त हों। जहां त्याग ही सब कुछ है और उसी में परम आनंद है। व्यावहारिक रूप में यदि हम इस प्रकार न्यूनतम वेतन कल्पना लेकर चलें तो फिर हमें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कर्म का परिश्रम यदि हम समाज को अर्पण कर देंगे तो हमारी चिंता कौन करेगा। तब समाज हमारी चिंता करेगा, क्योंकि हम समाज के अंग हैं और समाज का जब सामूहिक विकास होगा तो कोई कारण नहीं कि हमारा विकास न हो।
(पांचजन्य, अक्तूबर 21, 1957)