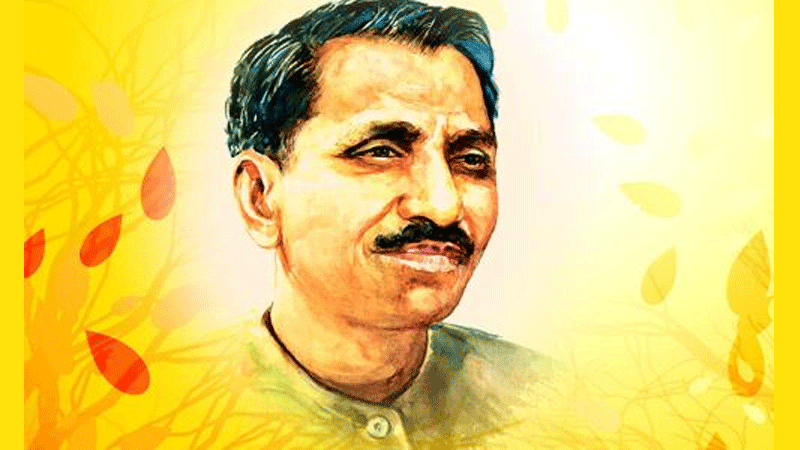पं. दीनदयाल उपाध्याय
जनवरी, 1965 में विजयवाड़ा में जनसंघ के बारहवें सार्वदेशिक अधिवेशन में स्वीकृत दस्तावेज
(गतांक से…)
आदेवमातृका कृषि
सिंचाई की योग्य व्यवस्था करना भारतीय शासन का सदैव से ध्येय रहा है। कृषि को आदेवमातृका बनाना शास्त्रों आदेश है। स्वातंत्र्योत्तर काल में यद्यपि बड़े-बड़े बांधों के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिये गए हैं, फिर भी अधिकांश कृषि इंद्रदेव की कृपा पर ही निर्भर है। छोटी योजनाओं की ओर दुर्लक्ष्य हुआ है। पुराने कुएं, तालाब, पोखरे आदि मरम्मत के अभाव में बेकार हो गए हैं।
सर्वतोमुखी दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत के लिए छोटे-छोटे सिंचाई के साधन ही उपयुक्त हैं। बड़े बांध पूंजी-प्रधान हैं। देश के अनेक भू-भागों में भूमि और जल-तल की ऐसी स्थिति है कि बड़े बांधों के कारण सेम और भूक्षार उत्पन्न होता है, जिससे भूमि के अनुर्वरा होने की आशंकाएं हैं। विद्यमान योजनाओं को छोड़कर आगे सामान्यतया छोटी योजनाएं ही हाथ में लेनी चाहिए। बड़ी योजनाओं में लगी पूंजी की शीघ्र वसूली की चिंता में सिंचाई एवं अन्य करों की दरें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसान उन्हें दुर्वह समझकर सिंचाई के साधनों का उपयोग ही न करें। छोटी योजनाओं में नलकूप बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
भूधृति
कृषि उत्पादन का संबंध कृषक से भी होता है। खेत और खेतिहर इन दोनों का एक अविभाज्य संबंध है। भूमि में सुधार करने तथा अधिकाधिक श्रम से अधिकतम उत्पादन करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान को इस बात का विश्वास हो कि वह भूमि से हटाया नहीं जाएगा तथा पैदा की हुई फसल का अधिकांश भाग उसका अपना ही होगा। विभिन्न ऐतिहासिक कारणों से भारत की भूमि व्यवस्था में बहुत से मध्यस्थों का समावेश हो गया है। जमींदार और जागीरदार अब समाप्त कर दिए गए हैं, किंतु
सर्वतोमुखी दृष्टि से विचार किया जाए तो भारत के लिए छोटे-छोटे सिंचाई के साधन ही उपयुक्त हैं। बड़े बांध पूंजी-प्रधान हैं। देश के अनेक भू-भागों में भूमि और जल-तल की ऐसी स्थिति है कि बड़े बांधों के कारण सेम और भूक्षार उत्पन्न होता है, जिससे भूमि के अनुर्वरा होने की आशंकाएं हैं
रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, जो स्वयं खेती नहीं करते, बल्कि दूसरों को पट्टे पर देकर उनसे फसल का निश्चित भाग लेते रहते हैं। कानून में वे कृषक हैं और कृषि के नाम पर मिलनेवाली सुविधाएं उन्हें ही प्राप्त होती हैं। फलत: वास्तविक कृषक निर्धन एवं सुविधाहीन बना हुआ है। कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि वास्तविक किसान को भूमि का मालिक बनाया जाए। कुछ राज्यों में, जहां इस प्रकार के क़ानून बने हैं, उनका ठीक-ठीक पालन नहीं हुआ। गैर-कानूनी, बेदखली या मरती से खेत छोड़ने के मामले बहुत ज्यादा है। आवश्यकता है कि काग़ज़ों में सुधार हो तथा कानून की भावना के अनुसार उसका पालन हो।
जोतने वाले की भूमि
व्याख्या—’जोतनेवाले की भूमि’ का यह अर्थ कदापि नहीं कि अपनी मेहनत को छोड़कर किसान किसी दूसरे की सेवाओं से लाभ नहीं उठा सकता। उसे आवश्यकतानुसार मजदूर रख सकने का अधिकार होना चाहिए, अन्यथा खेती चौपट हो जाएगी। ‘जोतनेवाले’ का साधारण अर्थ यही हो सकता है कि वह खेती के हानि-लाभ के लिए उत्तरदायी हो, उसमें पूंजी लगाता हो, वहां परिश्रम करता हो तथा उसकी देखभाल करता हो।
ऐसी अवस्थाएं भी हो सकती हैं, जब किसी कारणवश किसान एक या दो वर्ष के लिए खेती न कर सकता हो। यदि उस अवस्था में वह अपनी ज़मीन दूसरों को कुछ समय के लिए खेती करने के लिए नहीं दे सकेगा तो वह या तो खेत को बिना बोए हुए छोड़ देगा या केवल कागजी कार्रवाई के लिए उस पर खेती करेगा। इसका परिणाम कृषि उत्पादन के गिरने के रूप में होगा। अत: हमें कुछ अपवाद अवश्य करने होंगे। अवयस्कों, विधवाओं, अपंगों तथा फ़ौज के लोगों को भी इस नियम से मुक्त रखना होगा।
इसी प्रकार अलाभकर जोत वाले किसानों को अपना खेत पट्टे पर देने और लेने का अधिकार होना चाहिए।
अधिकतम जोत
सघन खेती की अनिवार्यता के कारण हमें एक और आर्थिक जोतों की व्यवस्था करनी होगी तथा दूसरी ओर जोत की अधिकतम मर्यादाएं भी बांधनी होंगी।
कृषि स्वामित्व
सहकारी या सामुदायिक खेती भारत के भूमि-जन अनुपात, प्रजातंत्रीय पद्धति, बेकारी का निवारण, प्रति एकड़ अधिकतम उत्पादन, कृषि में मानकों के निर्धारण की असंभवनीयता, किसान का भूमि-प्रेम एवं हमारे जीवन-मूल्य, इन सभी दृष्टियों से हमारे लिए अनुपयुक्त है। कृषक स्वामित्व ही भूमि व्यवस्था का आधार होना चाहिए।
वन देश की बहुमूल्य संपत्ति हैं। उनका प्रभाव देश की जलवायु एवं वर्षा पर भी पड़ता है। उनका ह्रास रोकने, संरक्षण एवं रोपण के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वन और वनवासी दोनों ही पिछले अनेक वर्षों से बुरी तरह शोषण के शिकार हुए हैं। वनवासी को खेती के लिए भूमि देना तथा वनों से आजीविका चलाने की सुविधा पुनः देना आवश्यक है
चकबंदी
भूमि का अंतर्विभाजन एवं अपखंडन भी भारतीय कृषि की एक समस्या है। इसे चकबंदी द्वारा रोकने के प्रयास किए गए हैं। जिन तरीक़ों और क़ानूनों के अंतर्गत चकबंदी की जा रही है, उनमें पक्षपात एवं भेदभाव के लिए बहुत गुंजाइश है। गांव का मास्टर प्लान बनाकर चकबंदी करनी चाहिए। जिनके चक छोटे हैं, उन्हें भूमि देते समय यह ध्यान रखा जाए कि वे उन्हें लाभकर बना सकें।
आर्थिक जोत से नीचे अंतर्विभाजन और अपखंडन पर रोक लगा दी जाए।
खेतिहर मज़दूर
कृषि में खेतिहर मजदूर का सहयोग सदैव आवश्यक रहेगा। उसको पूरी मजदूरी, वर्ष भर काम तथा ग्रामवासियों को मिलनेवाली सभी सुविधाएं मिल सकें, इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु गांवों में सहायक उद्योगों की स्थापना आवश्यक है।
गोवंश की अवध्यता
गोवंश के प्रति भारतीय जनता की भावनाओं का समादर करने तथा उसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान होने के कारण उसके संरक्षण एवं संवर्धन पर अत्यधिक बल देना चाहिए तथा गोवंश हत्या पर वैधानिक प्रतिबंध लगाना चाहिए। मिश्रित कृषि भारत के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
विपणन
उत्पादन वृद्धि के कार्यक्रमों के साथ ही कृषि माल के विपणन एवं ऋण की व्यवस्था भी करनी होगी। अभी तक गांव का साहूकार कुछ अंशों में ये कार्य करता है। किंतु बाजारों की अच्छी व्यवस्था न होने के कारण किसान को कभी उचित दाम नहीं मिल पाया है। कच्चे माल के कम दामों के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही मूलत: दोषी है। इसमें कच्चे माल और पक्के माल के मूल्यों के बीच कोई तालमेल नहीं। अतः किसान के साथ न्याय करने के लिए आवश्यक है कि गांवों में कोठार एवं गोदाम बनाए जाएं, जिससे किसान को अपनी फसल की साख पर योग्य ऋण प्राप्त हो जाएं। सहकारी समितियां यह काम भली-भांति कर सकती हैं। कृषि बीमा योजना भी उपयोगी सिद्ध होगी।
वन
वन देश की बहुमूल्य संपत्ति हैं। उनका प्रभाव देश की जलवायु एवं वर्षा पर भी पड़ता है। उनका ह्रास रोकने, संरक्षण एवं रोपण के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। वन और वनवासी दोनों ही पिछले अनेक वर्षों से बुरी तरह शोषण के शिकार हुए हैं। वनवासी को खेती के लिए भूमि देना तथा वनों से आजीविका चलाने की सुविधा पुनः देना आवश्यक है।
उद्योग नीति
देश के औद्योगीकरण की अपरिहार्यता निर्विवाद है, किंतु उसकी गति कितनी और स्वरूप कैसा हो, यह मतभेद का विषय है। सामान्यत: पश्चिम के औद्योगिक ढांचे को ही एकमेव ढांचा मानकर उसे जल्दी-से-जल्दी देश में लाने की आतुरता दिखती है। विदेशी पूंजी के सहयोग ने इस निर्णय को और भी प्रभावित किया है। अभी तक इस प्रकार का जो औद्योगीकरण हुआ है, उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हुई है, किंतु दूसरी और पुराने उद्योग नष्ट होकर निरुद्योगीकरण एवं विपूंजीकरण हुआ है, बेकारी बढ़ी है, विदेशों पर निर्भरता तथा विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है, केंद्रीयकरण तथा आर्थिक विषमताएं अधिक हुई हैं तथा तेजी से होनेवाले नगरीकरण एवं अपने घर और गांव से दूर बड़े-बड़े शहरों में समाज-संबंध-विहीन जनसमुदाय के केंद्रीकरण से अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। हम इन समस्याओं को औद्योगीकरण के स्वाभाविक परिणाम कहकर नहीं टाल सकते।
(क्रमश:…)